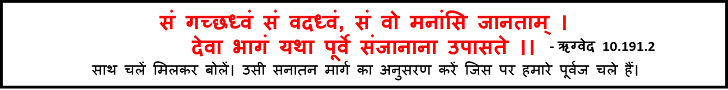छान्दोग्य उपनिषद् में एक कथा मिलती है कि एक बार शरीर की इंद्रियों में विवाद छिड़ गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। वे लड़ती हुई इस झगड़े के निपटारे के लिए प्रजापति के पास पहुँचीं। प्रजापति ने कहा इसका निर्णय परीक्षा से हो। जिसके चले जाने पर शरीर सबसे अधिक कुरूप तथा अपवित्र दिखाई पड़े, वही सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी।
इस परीक्षा के लिए सबसे पहले वाणी को एक वर्ष के लिए शरीर से बाहर निकाला गया। शरीर ने कहा कि गूँगे लोग भी मजे से देखते, सुनते, खाते–पीते हैं। इसके बाद क्रम से वाक्, आँख, कान तथा मन आदि को बारी–बारी एक–एक वर्ष के लिए बाहर निकाला गया, उस पर भी शरीर का उत्तर वैसा ही मिला।
अन्त में निकलने की बारी आई प्राण की! तब ऐसा लगा जैसे अच्छा घोड़ा अपने पैर बांधने के कीलों को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार प्राण सभी इंद्रियों को जड़ से उखाड़ डाल रहा है।
अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥
अथ हैनँश्रोत्रमुवाच यदहं सम्पदस्मि त्वं तत्सम्पदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥
– छान्दोग्योपनिषद् ५.१.१३–१४
इस समय वाणी ने प्राण से कहा कि जो मैं ‘वसिष्ठ’ कही जाती हूँ, वह सचमुच तुम्हीं हो। आँखों ने कहा कि जो मुझे ‘प्रतिष्ठा’ कहते हैं, वह प्रतिष्ठा मात्र तुम्हीं हो। कानों ने कहा कि जो मुझे ‘सम्पद्’ कहा जाता है, वास्तव में तुम्हीं हो। मन ने कहा कि जो मुझे जीवन का ‘आयतन’ या ‘आधार’ कहते हैं, वह मात्र तुम्हीं हो।
अब यहाँ हमारे मन में यह एक प्रश्न उठ सकता है कि प्राणों के महत्व को समझाने के लिए उपनिषत् को ऐसी परीक्षा क्यों आयोजित करनी पड़ी?
विचार करने पर ज्ञात होता है कि यही जीवन की एक मात्र सच्चाई है। जो हमारे जीवन का अनिवार्य है, जो सुन्दरतम है, वह हमारी आँखों से ओझल रहता है। उस ओर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है। आँख, कान आदि को बंद करके उसके महत्व को तो हम समझ सकते हैं। किन्तु प्राण के महत्व को बिना विचार नहीं समझा जा सकता।
संस्कृत भाषा में प्राण के लिए जो शब्द विकसित हुए, वे अवस्थिति या प्रतिष्ठा के ही द्योतक हैं। ‘प्राण’ शब्द का मूल अर्थ यही है। अन्य ‘असु’ शब्द ‘अस्’ धातु से विकसित है, जिसका अर्थ ‘होना’ मात्र है। निरुक्त के अनुसार असु + र अर्थात् ‘प्राणों वाला’ इस यौगिक अर्थ में असुर का प्रयोग होता है। (अपि वाऽऽसुर इति प्राणनाम, अस्तः शरीरे भवतितेन तद्वन्तः – निरुक्त ३.८)
वेद में इसी मौलिक व्युत्पत्ति के अनुसार असुर शब्द का प्रयोग मिलता है (स्वस्ति पूषा असुरो दधातु… ऋग्वेद५.५१.११ में सूर्यदेव को असुर कहा गया है) तथा अवेस्ता भाषा में ‘अहुर’ शब्द का देवता अर्थ में प्रयोग हुआ है।
इसी प्रकार विश्व में सूक्ष्म से विशालतम जन्तुओं के प्राण को ही प्रतिष्ठा स्वरूप मानते हुए उन्हें एक सामान्य नाम दिया गया – ‘प्राणी’। अर्थात् ये सभी प्राण ग्रहण करने वाले हैं।
विदेशों में इन्हीं जन्तुओं के लिये एक नाम ‘animal’ प्रदान किया गया जो लैटिन भाषा के ‘animale’ शब्द से विकसित है जिसका अर्थ है ‘श्वास ग्रहण करने वाला’। अंग्रेजी में भी ‘animate’ क्रिया का श्वास लेने के अर्थ में प्रयोग होता है।
यद्यपि आजकल हम सभी animal का अनुवाद ‘चौपाए पशु’ करते हैं किन्तु जन्तु–विज्ञान के अनुसार विस्तृत अर्थों में protozoa जैसे एक कोशकीय सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालतम जन्तु भी श्वास ग्रहण करने की योग्यता के कारण animal के अन्तर्गत ही आते हैं।