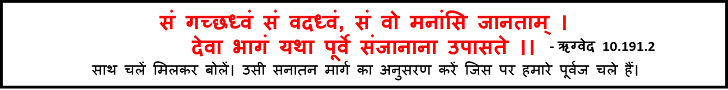वेदान्तदर्शन के तीन उपजीव्य स्तम्भ हैं, इन्हीं तीनों को सभी प्राच्य और प्रचित्य विद्वान वेदान्त की ‘प्रस्थानत्रयी’ के नाम से जानते हैं। ये हैं :
- श्रुति (उपनिषद)
- स्मृति (श्रीमद्भगवद्गीता)
- सूत्र (ब्रह्मसूत्र)
१. श्रुति : वेद के ज्ञानकाण्डीय श्रुतियों का संकलन ‘उपनिषदों’ के नाम पर किया जाता है। इनमें से वेदान्तदर्शन के सैद्धांतिक विचारों के साथ प्रायशः बीस उपनिषदें एक वक्यतापन्न हुई हैं। इसी वेद भाग को वेदान्तदर्शन का प्रथम प्रस्थान कहा जाता है।
२. स्मृति : वेदान्तदर्शन की स्मृति है श्रीमद्भगवद्गीता! जो साक्षात् पूर्ण परात्पर ब्रह्म परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। श्रीमद्भगवद्गीता को उपनिषदों का सार कहते हैं, यह भारतीय ज्ञान–विज्ञानकोश का एक ऐसा अमूल्य भण्डार है जिसे हम प्राजापत्यशास्त्र (वेदशास्त्र) के ज्ञानविज्ञानात्मक पारिभाषिक रहस्यपूर्ण विषयों का ‘सूचीग्रंथ’ कह सकते हैं।
वेदशास्त्र की तात्विक परिभाषाएँ – १. ब्रह्म तथा २. यज्ञ भेदसे दो स्वतंत्र धाराओं में प्रवाहित हैं।
ब्रह्मतत्व का विश्लेषण करने वाली परिभाषाएँ ज्ञान प्रधान हैं एवं यज्ञतत्व का विश्लेषण करने वाली परिभाषाएँ विज्ञान प्रधान हैं। अर्थात् ज्ञान का ब्रह्म से सम्बंध है और विज्ञान का सम्बंध यज्ञ से है, जैसा कि ‘ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा’ (शतपथ ब्रा० ६.१.१.८) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। इसमें भी मूल विद्या ब्रह्मविद्या है और तूलविद्या यज्ञविद्या है। केंद्रविद्या मूलविद्या है और पृष्ठविद्या तूलविद्या है। ज्ञानप्रधाना ब्रह्मविद्या ही मंत्रविद्या है एवं विज्ञानप्रधाना नानात्त्वनिबन्धना पृष्ठया यज्ञविद्या ही ‘ब्राह्मणविद्या’ है। मंत्रविद्यात्मक वेद भाग ही मूल वेद हैं, सूत्र वेद हैं एवं ब्राह्मणविद्यात्मक वेद भाग ही तूल वेद हैं, व्याख्यावेद हैं। ब्रह्म की व्याख्या ही ब्राह्मण है।
दोनों के अतिरिक्त विद्या की और कोई स्वरूप-व्याख्या शेष नहीं रह जाती। दोनों के परिज्ञानानन्तर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता। यही वेद शास्त्र की परिपूर्णता है जिसका सर्वात्मना एकमात्र गीताशास्त्र ही प्रातिनिध्य कर रहा है, जैसा कि गीता ७.२ के प्रतिज्ञासूत्र से प्रतिध्वनित है —
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥
– श्रीमद्भगवद्गीता ७.२
अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं – मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित ज्ञान सम्पूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा।
इस प्रकार समझने पर यह ज्ञात होता है कि श्रीमद्भगवद्गीता सर्वशास्त्रमयी है किन्तु यह एक सूचीग्रंथ है। सब कुछ श्रीमद्भगवद्गीता में समाहित है किन्तु सूत्र रूप में; जिसे पूर्ण रूप से समझने के लिए साधक का योग्य होना अत्यंत आवश्यक है। बिना योग्यता के स्थिति वही होगी जो दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को दसवीं की पुस्तक दे दी जाए।
३. सूत्र : वेदान्त दर्शन का सूत्र है ब्रह्मसूत्र! इसके प्रणेता स्वयं भगवान वेदव्यास हैं। यही वेदान्त का तृतीय प्रस्थान है।
इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, श्रीमद्भगवद्गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान भी कहते हैं।
प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरू अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिये सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था; और उसी को स्वसम्प्रदायाचार्य और जगद्गुरु पद पर अभिषिक्त किया जाता था जो अपने सम्प्रदाय में स्वीकृत वाद को आधार मान कर देवभाषा संस्कृत में वेदान्त की प्रस्थानत्रयी पर विद्वत्सम्मत प्रौढ़भाष्य की रचना कर लेता था।
इन्हीं तीनों पर अपनी – अपनी चिन्तन परम्परा के अनुसार आचार्यों ने अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और अचिन्त्याभेद नामक छः वादों को प्रस्तुत कर विपुल दार्शनिक सामग्री से भारतीय संस्कृति की पूजा व आराधना की है।
क्रमशः ..